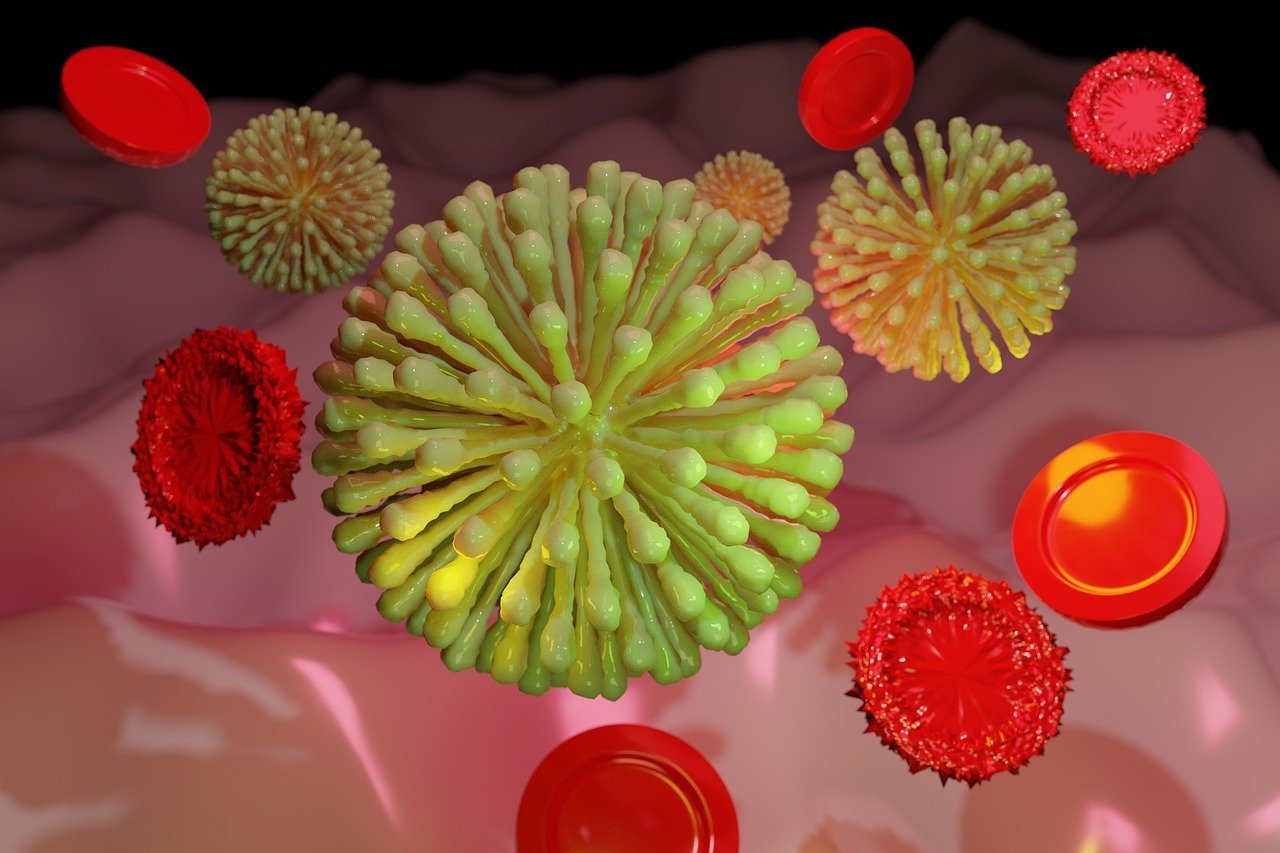यहाँ कोरोना के पहले हफ्ते में हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये फैक्ट्री वाले लोग थे। जनकल्याणकारी राज्य है, तो यह रूटीन प्रक्रिया है। सरकार बेरोजगारी भत्ता देती ही है, और कंपनी के घाटे की भी ठीक-ठाक भरपाई कर देती है। और चूँकि सरकार ऐसा करती है, तो कंपनी भी नौकरी से निकालने में एक दिन भी देर नहीं करती। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, तो ज़रूर कंपनी चार बार सोचती। इस खेप में ‘ब्लू कॉलर’ (मजदूर, मशीन-कर्मी वर्ग) को निकाल दिया गया, और ‘व्हाइट कॉलर’ को आधा निकाला गया। यानी आधी वेतन दी जाने लगी (और कुछ सरकार भी देने लगी)। तीसरे हफ्ते तक यह भेद भी खत्म कर दिया गया, और धड़ाधड़ ‘व्हाइट कॉलर’ लोग निकाले जाने लगे जो अभी चल ही रहा है। बाकी, कॉन्ट्रैक्ट पर और फ्रीलैंसर लोगों का तो कोई माई-बाप नहीं। उनको सरकार भी ख़ास सहयोग नहीं दे पाती।
जो वेलफेयर-स्टेट नहीं हैं, वहाँ बीमा है। आज बी.बी.सी. पर रिपोर्ट आयी है कि अमरीका ने 2008 की मंदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पिछले हफ्ते तक पैंतीस लाख लोग नौकरी से निकाले गए। बीमा विशेषज्ञों ने इसे बेरोजगारी का पैन्डेमिक बनने की चेतावनी दी है। आखिर बीमा कंपनी भी कितने बेरोजगारों का जिम्मा उठा पाएगी? और कब तक?
भारत में कुछ मिली-जुली व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी लॉकडाउन से पहले ही ‘ब्लू कॉलर’ सड़क पर आ ही गए। बंबई-दिल्ली से ट्रेन पकड़ कर, और बाद में पैदल निकल पड़े। ‘व्हाइट कॉलर’ पर अभी गाज पड़नी शायद नहीं शुरू हुई हो। लेकिन, उनका बड़ा हिस्सा पहले भी अमरीका पर निर्भर रहा है। तो यह प्रभाव सुनिश्चित ही है। भारत अब बड़े तौर पर खुली अर्थव्यवस्था है और हर क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रवेश कर चुका है। इसलिए, उनके गिरते ही हमारी अर्थव्यवस्था भी गिरेगी ही। अगर कह दिया जाए कि सबको कुछ दिन नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन जान बचाने के लिए लॉकडाउन जारी रखें तो? क्या हम अवैतनिक अपनी और दूसरों की जान बचाना जारी रखेंगे?
खैर, यह सब बातें तो मुझे भी किसी और ने बतायी। मेरी चिंता तो इसके मानसिक प्रभाव पर है। अभी से यह हालात बनने लगे हैं कि लोग कह रहे हैं, हम काम पर लौटेंगे। रिस्क लेने को तैयार हैं। और यह आवाज़ ‘व्हाइट कॉलर’ वालों की तरफ से आ रही है। वे मनोविशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। अभी सरकार ने तीस प्रतिशत तक प्रोडक्शन शुरू करने की बात कही है, जिसमें मूलत: निचले पायदान के कर्मियों की ही जरूरत होगी। ऊपरी पायदान यानी ऑफिस में बैठने वाले तो देर से आएँगे। महामारी को देखते हुए, यूँ मनमर्जी फैसला लेना भी कठिन है कि फुल प्रॉडक्शन चला दिया। कम बजट, कम मैनपावर से ही काम चलाना पड़ेगा।
इसका एक विचित्र हल भी सोचा जा रहा है। ‘डेथ-कैप’ तय करना। जैसे मान कर चलना कि दो लाख लोग मरेंगे, और टेस्ट बंद कर देना। गिनती रोक देना। चीन ने ढोल पीट कर कह दिया कि गिनती बंद। पाकिस्तान-अफग़ानिस्तान, अफ्रीका के अधिकतर देश, तो यह तय कर ही चुके हैं। यूरोप में भी यह संभव है। कम से कम यहाँ के स्वास्थ्य-मंत्री की बातों से यही लगता है कि जनता-जाँच के बजाय चिकित्सक-निर्धारित जाँच ही चलेगी। जैसा अन्य बीमारियों में चलता है। केस टू केस।
यह एक तरह की मांडवली है धन और जीवन के बीच। बैलेंस बनाना कि दुनिया चलती रहे। नयी दुनिया के प्रमेय में थोड़ा चेंज है। जान नहीं भी है, जहान तो है।
(प्रवीण झा नार्वे के एक अस्पताल में डॉक्टर है. वे चिकिस्ता से लेकर साहित्य विषयों के अग्रणी और लोकप्रिय लेखक हैं.)